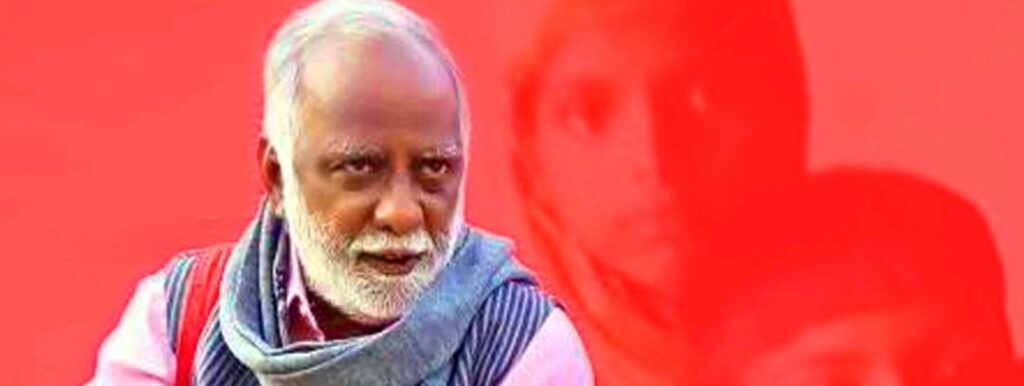तीन महीने पूरा कर चुकी ‘भारत जोड़ो’ यात्रा 20 नवम्बर को सप्ताह भर के लिए मध्यप्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। यह यात्रा हमारे कालखंड की एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट घटना है। इसे सरासर खारिज करने या दोनों बाँहें फैलाकर गले लगाने की दोनों अतियों से बचते हुए इसे पायथागोरस की मशहूर प्रमेय : त्रिभुज के तीनो कोण मिलकर दो समकोण के बराबर होते हैं, की तर्ज पर तीन कोणों से देखना ठीक रहेगा।
लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य “भारत दैट इज इंडिया” के नागरिक के नाते देखें, तो हमारा समय जटिल समय है ; यह समय घुटन का समय है। किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज के लिए सबसे जरूरी है खुलापन, बेबाक बहस, असहमति और प्रतिरोध। भारत और दुनिया में समाज इन्हीं की दम पर आगे बढ़ा है, आगे बढ़ता है। हाल के दौर में, खासकर 2014 के बाद से यह लगभग गायब है। एकपक्षीय गरल का प्रवाह है। बेहिचक संवाद तो दूर, बोलने और लिखने के कामों को भी अघोषित रूप से लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मीडिया, शिक्षा, विश्वविद्यालय, मंदिर हर माध्यम पर जॉर्ज ऑरवेल का बिग ब्रदर खाकी नेकर पहने लाठी लिए बैठा है। वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उसके कहे की समीक्षा नहीं की जा सकती। इस देश में ईश्वर से प्रश्न किये जा सकते हैं मगर यह बिग ब्रदर जो भी कहे, उसको लेकर कोई सवाल–जवाब नहीं किये जा सकते। सूचना और कम्युनिकेशन के हर माध्यम पर वर्चस्व कायम कर लिया गया है। अब सिर्फ अमावस की बात करनी है, उसकी सराहना करनी है। पूर्णिमा तो दूर रही – मोमबत्ती या दीपक जलाना भी अपराध है ; राष्ट्रद्रोह है।
यह हमला सर्वग्रासी है, सर्वआयामी है ; निशाने पर सिर्फ वर्तमान नहीं है।अतीत भी है। पिछले 5 हजार वर्षों में भारतीय समाज की जड़ता पर हुए प्रहारों से जो सामाजिक समझ, संस्कार और साझा विवेक हासिल हुआ है, उसे वापस लौटाने की मुहिम है। अब तक के सारे सकारात्मक हासिल का निषेध है। इसलिए यह मसला सिर्फ चुनावी हार–जीत का नहीं है। ’दूबरे के दो आषाढ़’ की तर्ज पर यह समय सन्निपात का भी समय है। उधर हड़बड़ी है – एक फासिस्ट राज कायम करने की जल्दबाजी है, तो इधर भी झुंझलाहट है। चिड़चिड़ापान है, खुद को एकमात्र सही मानने और बाकी सब कुछ को खारिज कर देने का भाव है। समग्रता में मूल्यांकन का विवेक गायब हो रहा है। ऐसे में अनेक प्रयासों की तरह यह “भारत जोड़ो” यात्रा इस प्रायोजित और जानबूझकर रचे गए सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश है। इसीलिए यह हमारे कालखंड की एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट घटना है।
एक पत्रकार और सम्पादक के नाते दूसरे कोण से देखने पर कुछ सवाल भी सामने आते हैं। वैसे यकीनन इसने हुक्मरानों और उनके रिमोटधारियों के बीच बेचैनी और चिंता पैदा की है। वे इसके संभावित असर से घबराये हुए हैं। इसके मीडिया कवरेज को हस्बेमामूल राजा का बाजा बजाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके जरिये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और यह यात्रा उस झांसे में फंस रही है। जैसे इस यात्रा को भारत की जनता की यात्रा, भारत की सलामती के प्रति चिंतित, इसकी एकजुटता और बेहतरी के लिए आतुर और प्रयत्नशील व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, सिविल सोसायटी की यात्रा के रूप में शुरू करने की बात थी।
मीडिया ने पहले ही दिन से इसे एक पार्टी विशेष की यात्रा बना दिया और तीसरे–चौथे दिन से इसे एक व्यक्ति – राहुल गांधी – की यात्रा में बदल दिया। उन्हें यह करना ही था। वे सब कुछ फलां विरुद्ध फलां तक सीमित और संकुचित करके रख देना चाहते थे — इससे उनका काम आसान हो जाता है। व्यक्तियों की मार्केटिंग के धंधे के वे पक्के खिलाड़ी हैं। माफीखोरों को वीर और हत्यारों को शांतिदूत तक बनाने और नायकों को खलनायक बनाना उन्हें अच्छी तरह आता है।
ऐसी स्थिति में इस व्यापकता को सुनिश्चित करने की जिद आयोजकों में होनी चाहिए थी, मगर कुछ सदाशयता से कहें तो, वे उकसावे में आ गए और जैसा शकुनि चाहते थे, उसी के हिसाब से खेल गए और इस यात्रा को एक व्यक्ति की यात्रा में घटा कर रख दिया गया। इस अभियान के प्रचारतंत्र ने भी व्यापक भागीदारियों की अनदेखी की। व्यक्ति की बजाय मुद्दों को जो प्रोजेक्शन और स्पेस देना चाहिए था, वह कथित मेन स्ट्रीम मीडिया को तो तो नहीं ही देना था, खुद आयोजकों के प्रचारतंत्र ने भी नहीं दिया। यह भुला दिया गया कि अब – 2014 के बाद से – लड़ाई रूप में ही नहीं, सार में भी भिन्न हुयी है ; उसके मुकाबले के लिए जो तरीके अपनाने होंगे, वे नए होंगे, अब तक आजमाए गए तरीके नहीं होंगे, रूप और सार दोनों में भिन्न और समावेशी होंगे।
एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते देखे, तो पहली बात दिशा की है। 07 सितंबर, 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुयी इस यात्रा को मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, राजनीतिक केंद्रीकरण और विशेष रूप से “भय, कट्टरता” की राजनीति और “नफरत” के खिलाफ लड़ने के लिए अभियान बताया गया। अच्छी बात है। मगर विकल्प क्या है? विकल्प सरकार बदलना भर है? चलिए बदल दी – इसके बाद क्या होगा? जिन दरियाओं की चपेट में आज पूरा समाज और देश है, क्या उन्हें सिर्फ भावनात्मकता और भावुकता के तिनकों से टाला जा सकता है? जाहिर है कि नहीं ; अंधेरों को कोसना काफी नहीं होता, उन्हें चूर–चूर करने के लिए उजाला भी करना होता है ; वैकल्पिक नीतियां भी लानी होती हैं।
बदलाव व्यक्तियों या दलों के नहीं, नीतियों के होते हैं। वैकल्पिक नीतियां ही वह क्रिटिकलिटी पैदा करती हैं, जिससे अपार ऊर्जा बनती है। जहां, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि में उन्हें लागू कर सकते हैं, वहां अमल में लाकर उदाहरण भी प्रस्तुत करना होता है। मंदसौर में 2017 में किसानों पर चली गोलियों के बाद निकली किसान संगठनों की यात्रा ने महज दो–ढाई वर्ष में देश के किसानों को जगाकर साढ़े तेरह महीने के लिए दिल्ली की बॉर्डर पर खड़ा कर दिया था – इसलिए कि वह बाकायदा एक विकल्प लेकर निकली थी। इस यात्रा से पहले देश के चार कोनों से निकली अखिल भारतीय किसान सभा की यात्राओं ने इन नीतियों को देश के किसानों की चेतना में ला दिया था। मुक्तिबोध के यक्ष प्रश्न “पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?” का जवाब इस यात्रा को अभी साफ़–साफ़ तरीके से सूत्रबद्ध करना है।
दूसरी बात असली दुश्मन की शिनाख्त और उसके मुताबिक़ खर्च किए जाने वाले समय के अनुपात की है। देश की एकता, सम्प्रभुता, भाईचारे पर लपकने वाला और बहुमत जनता के जीवन के हर आयाम पर झपटने वाला भेड़िया कहाँ है? हांका और हुंकार उसी अनुपात में तो होगी। जहां टूटन ज्यादा है, जोड़ना वहीं से शुरू होगा। यात्रा का मार्ग इससे मेल नहीं खाता। केरल में 18 दिन, गुजरात में 0, यूपी में 3-4 दिन, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में एक सप्ताह या सप्ताह से भी कम!! ये कौन सा अनुपात है? यही हाल आंध्रा, तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र का है। समस्या सिर में हैं, मरहम पट्टी पाँव की जा रही है। विघटन और विग्रह के राक्षस की जान जिस कौए में है, वह जहां बसता हैं, उस ओर पाँव तक नहीं बढ़ रहे, जहां से उसे स्थायी रूप से खदेड़ा जा चुका है, उस कोयलों के केरल में धमाधम हो रही है।
तीसरी बात प्राथमिकता की है। कन्याकुमारी से कश्मीर का रास्ता 1983 में चंद्रशेखर ने भी चुना था। मगर 1983 और 2022 में गुणात्मक फर्क है। आज कश्मीर में वह सब दांव पर लगा है, जो “भारत दैट इज इंडिया” की आधारशिला है। आज जो कश्मीर में हो रहा है, उसे यदि होने से नहीं रोका गया, तो कल वह पूरे देश में होगा। गांधी को ही देख लेते। 1915 में भारत आकर उन्होंने कहाँ से शुरू किया था – चम्पारण से। आजादी के वक़्त हुयी अशांति के वक्त वे कहाँ थे – नोआखाली और कोलकता में। सबसे मुश्किल शुरुआत ही सबसे मजबूत शुरुआत होती है। आम कहावत है कि मरखने सांड़ को सींग से पकड़ा जाता है पूंछ से नहीं। इसी तरह धर्मनिरेपक्षता को धर्मनिरपेक्षता ही बोलना होगा। पतली गलियों की भूलभुलैयायें देखने में ऊपर ले जाती लगती हैं, लेकिन असल में कहीं नहीं ले जातीं।
यात्राएं वही सफल होती हैं, जो अपनी मंजिल ठीक तरह से चुनती हैं और उसके अनुरूप मार्ग निर्धारित करती है। अभी तक नहीं लगता कि इस यात्रा की कोई निश्चित मंजिल है, उस तक पहुंचने वाले रास्ते का कोई नक्शा है।
-बादल सरोज